एक सज्जन ने मुझे फोन किया। “जीडी, तुमने अमर उजाला देखा? सबसे ऊपर एक छोटे से कस्बा नुमा शहर के आदमी के देहावसान पर पूरे पेज का विज्ञापन है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मडीयाहू जैसे कस्बे के आदमी का दस-पंद्रह लाख खर्च कर कोई ऑबीच्यूरी छपायेगा।”
अमर उजाला मेरे घर आता नहीं, पर मैने प्रयास कर वह हासिल किया। कोई राम अचल पाण्डेय का जिक्र था उसमें।
वे सज्जन 96 वर्ष की उम्र पा कर एक दो दिन पहले दिवंगत हुये थे। काजीहद पंडान, मडियाहू, जौनपुर का पता लिखा है। मडियाहू कस्बा ही है जौनपुर जिले में। आबादी 40-50 हजार की होगी। अमर उजाला के अगर वाराणसी संस्करण भर में भी वह विज्ञापन हो तो भी उसका खर्च 10 लाख से कम न होगा। दस लाख विज्ञापन भर में तो तेरही और अन्य कर्मकांड में करोड़ों में खर्च! पूर्वांचल की गरीबी के बीच यह सम्पन्नता मुझे आकर्षित कर गई – किसी को भी कर सकती है।
मेरी कल्पना के अश्व भागने लगे। बेलगाम!
मैने कल्पना की। मैं नीलकंठ चिंतामणि हूं और उक्त विज्ञापन में वर्णित सज्जन कृष्ण मोहन हैं। अयोध्या से जनकपुर की राम की विश्वामित्र के साथ की गई यात्रा को मैं (नीलकंठ) ट्रेस कर रहा था साइकिल से; तब मडियाहू में मुलाकात हुई थी कृष्ण मोहन से। सामान्य सी साइकिल से जाता मैं और एक बड़ी सी कोठी नुमा घर में कृष्ण मोहन – शायद दोनो एक दूसरे से सामान्य विपन्नता और सम्पन्नता से अलग, एक दूसरे से प्रभावित हुये। मैं दो दिन उनके यहां रुक गया। वहीं लगा कि उनका जीवन वृत्तांत जानना और लिखना बहुत रोचक भी होगा और एक आदमी की फर्श से अर्श की सफलता को समझना अभूतपूर्व होगा। कृष्ण मोहन ने मुझे अपने कुछ व्यक्तिगत कागज दिये जिससे जान सकूं कि वे कैसे आदमी हैं।
उन्हीं कागजों में एक यह है।
अब जब कृष्ण मोहन नहीं रहे, तो मैं उसे शेयर कर सकता हूं। इसकी अनुमति, कि मैं उनके कागजों का अपने मन माफिक इस्तेमाल कर सकता हूं; कृष्ण मोहन ने मुझे दी थी… अब वह अनुमति इतिहास बन गई है।
कृष्ण मोहन के लेख पर मैं अपनी सोच भी लिखूंगा, उसके बाद, इस ब्लॉग पोस्ट में।
यह है कृष्ण मोहन का लेख –
मेरे (कृष्ण मोहन के) बारे में मेरी कलम
मैं जानता हूँ, मेरी कहानी लिखते समय सबसे कठिन प्रश्न यह नहीं होगा कि मैंने कितना कमाया, बल्कि यह होगा कि मैं कितना ठीक था और कितना ग़लत। यह प्रश्न मैं अपने लिए कभी बहुत साफ़ नहीं कर पाया, इसलिए बेहतर है कि इसे वैसे ही दर्ज कर दूँ — जैसे यह मैने जिया।
पूर्वांचल में नैतिकता कोई सीधी रेखा नहीं होती। यहाँ वह नदी की तरह है —
कहीं साफ़, कहीं गाद से भरी,
कहीं किनारे काटती हुई,
कहीं खेतों को सींचती हुई।
मैं उसी नदी के किनारे पला-बढ़ा।
- सिस्टम और मैं
देश आजाद हुआ ही था। और मैं कलकत्ता पंहुच गया था। कैसे पंहुचा और कितने पापड़ बेले, वह तो विस्तार से कोई सुपात्र सज्जन लिखेंगे। पर मैं सरकारी अमले के सम्पर्क में आया वहां।
सरकारी दफ्तरों में मैंने कभी यह नहीं पूछा कि काम क्यों नहीं हो रहा, मैंने यह पूछा कि काम कैसे होगा।
ओवरसियर, एक्सईएन, दारोगा, चुंगी वाले, जंगलात वाले; और भी अनेक लोग — ये लोग मेरे लिए व्यक्ति नहीं थे, ये प्रक्रिया के हिस्से थे।
मैंने उन्हें पैसा दिया। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता।
पर मैंने इसे चोरी नहीं माना, क्योंकि:
मैंने बिल बढ़ाकर नहीं बनाया; कंस्ट्रक्शन के काम में मैंने घटिया सामग्री नहीं लगाई; मैंने इमारतें और पुल गिरने नहीं दिए…
कदम कदम पर रिश्वत देनी थी। मेरे मन में रिश्वत पाप नहीं थी, काम बिगाड़ना पाप था।
अगर मेरा यह तर्क गलत है, तो यह गलती अकेले मेरी नहीं है। सर्व व्यापक व्यवस्था वही थी और अब भी है।
- दहेज और परिवार
मेरे दोनो बच्चों की शादी में बहुत कुछ आया। और मैंने मना नहीं किया।
यह भी उतना ही सच है कि मैंने माँगा भी नहीं।
हमारे समाज में यह फर्क बहुत मायने रखता है —
शायद बाहर से देखने वाले को यह चालाकी लगे,
पर भीतर से यह मर्यादा थी।
मैं जानता हूँ, आने वाले समय में
इसे कोई भी सही नहीं ठहराएगा।
पर मेरे समय में,
लड़के की पढ़ाई,
उसका काम,
उसके पिता की हैसियत —
सबका मूल्य तय होता था।
मैंने उस बाज़ार से बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं की। हां, मुझे संतोष है कि मैं किसी भी मानक से लालची नहीं था।
- दबंगई, या व्यवस्था?
गांव में काफी सफल हो कर लौटा। यहां मेरा नाम चलता था।
यह सच है।
पर मैंने कभी यह चाहा नहीं कि लोग मुझसे डरें।
मैं चाहता था कि लोग समझें —
कि झगड़ा यहाँ आकर रुकेगा।
अगर दो परिवार भिड़ते,
तो मैं पंचायत बैठाता।
अगर कोई ज़्यादा उछलता,
तो बिना हीलाहवाली के दारोगा या कोई और बड़ा हाकिम मेरा फोन उठा लेता।
यह ताक़त थी —
पर यह ताक़त रोज़ इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं थी।
जिस दिन ताक़त रोज़ लगानी पड़े,
समझ लीजिए कि इज़्ज़त खत्म हो चुकी है।
- मेरा नैतिक गणित
मैंने कभी खुद को संत नहीं माना।
और न ही मैं अपराधी महसूस करता हूँ।
मेरे लिए नैतिकता का गणित यह था:
घर सुरक्षित रहे; काम समय पर पूरा हो; किसी की जान मेरी वजह से न जाए; मेरे बच्चे गाँव छोड़कर शहर में सिर उठा सकें
अगर यह सब कुछ पूरी तरह साफ़ रहकर संभव होता,
तो शायद मैं वैसा करता।
पर पूर्वांचल में
बहुत साफ़ रहना भी एक तरह की बेईमानी है –
क्योंकि तब आप दूसरों को सिस्टम के हवाले छोड़ देते हैं।
- आने वाले लेखक के नाम
अगर तुम यह पढ़ रहे हो,
और मेरी जीवनी लिखने का सोच रहे हो,
तो मुझे बचाने की कोशिश मत करना।
बस यह याद रखना —
मैं अपने समय का आदमी था।
मुझे आज के तराज़ू पर मत तौलना,
और मुझे दानव बनाकर भी मत लिखना।
मैं उस धूसर इलाके में रहा
जहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं,
पर पूर्वांचल की ग्रे नैतिकता को,
बहुत कम लोग उसे यथावत स्वीकार करते हैं।
नीलकंठ का कथ्य
मैं कृष्णमोहन से कहाँ असहमत हूँ — और कहाँ चुपचाप सहमत
कृष्णमोहन से मेरी असहमति सैद्धांतिक नहीं है। वह किसी एक कर्म, एक फैसले या एक समझौते पर टिकती नहीं। मेरी असहमति मेरी अपनी जीवन यात्रा से आती है।
मैं हमेशा यह मानता रहा हूँ कि नैतिकता अगर थोड़ी भी ढीली हुई, तो वह फिसलन बन जाती है। और फिसलन पर खड़ा आदमी खुद को चाहे जितना संतुलित समझे, अंततः गिरता ही है। कौन बचा है उस फिसलन से?
कृष्णमोहन इससे सहमत नहीं होते।
उनकी नैतिकता सीढ़ी नहीं, ढलान है –
जहाँ आदमी पैर जमा कर नहीं, चलते हुए संतुलन बनाता है।
कृष्ण मोहन कुशल नट हैं जो पतली रस्सी पर अपने को साधे सिर पर बोझ लिये चलता है। और मैं जमीन पर भी सर्कोपीनिया ग्रस्त आदमी की तरह चलता हूं जो वजह-बेवजह ठोकर खाता रहता है।
यहीं से हमारी दूरी शुरू होती है।
1. जहाँ मैं असहमत हूँ
मैं मानता हूँ कि
गलत को “सिस्टम की मजबूरी” कह देना
गलत को थोड़ा और स्थायी बना देता है।
कृष्णमोहन ने रिश्वत दी,
और उसे स्वीकार भी किया —
यह उनकी ईमानदारी है।
पर उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि
इस ईमानदारी की कीमत
किसी और ने चुकाई होगी या नहीं।
शायद किसी छोटे ठेकेदार ने,
जो “खर्चा” नहीं दे सका।
शायद किसी कर्मचारी ने,
जिसकी सी.आर. पूरी ईमानदारी के बावजूद खराब होती रहीं,
केवल इसलिये कि वह ठेकेदार से सही से काम न ले पाया।
मेरी रुक्ष नैतिकता
इसी सवाल पर अटक जाती है।
मैं यह नहीं कह पाता कि
“सब ऐसा करते थे”
ऐसा कहने पर,
मेरे अनुसार अर्थ यह है कि
“ऐसा करना बिल्कुल ठीक था”।
2. जहाँ मेरी असहमति थक जाती है
लेकिन यहीं,
कुछ दूर चलने के बाद,
मेरी असहमति थक भी जाती है।
क्योंकि मैं यह भी जानता हूँ कि
मेरी अपनी नैतिकता
मुझे अक्सर अलग-थलग कर देती है।
मैंने कई बार
साफ़ रहने की कीमत
अकेले रहकर चुकाई है।
कृष्णमोहन ने यह कीमत नहीं चुकाई।
उन्होंने समाज के साथ सौदा किया,
और समाज ने उन्हें जगह दी।
यह फर्क
न छोटा है,
न अनदेखा करने लायक। कृष्ण मोहन सफल है।
उसकी ऑबिच्युरी में पूरा फ्रंट पेज रंगा है।
मेरे जाने पर कोई ऑबीच्यूरी होगी ही नहीं!
3. दहेज, दबंगई और जीवन का शोर
दहेज पर मैं उनसे असहमत हूँ।
पूरी तरह।
पर सच यह भी है कि
मेरी असहमति ने
किसी व्यवस्था को नहीं बदला।
कृष्णमोहन की स्वीकृति ने भी नहीं बदला,
पर उसने उन्हें
अपने समाज में निर्वासित भी नहीं किया।
यह तथ्य मुझे असहज करता है।
गांव की हल्की दबंगई,
फोन उठाने भर की ताक़त —
यह सब मुझे स्वीकार नहीं।
पर मैं यह भी देखता हूँ कि
कृष्णमोहन के गांव में
अराजकता नहीं थी।
लोग कृष्ण मोहन को जानते थे और पसंद भी करते थे।
मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं है।
यह कोई नैतिक जीत नहीं है,
पर यह जीवन की एक सच्चाई ज़रूर है।
4. अगर जीवन फिर से जीना हो…
यहीं मैं सबसे ईमानदार होना चाहता हूँ।
अगर जीवन फिर से जीना हो,
तो मैं नहीं जानता कि
मैं पूरी तरह कृष्णमोहन बन पाऊँगा या नहीं।
पर मैं यह जानता हूँ कि
मैं अपने जैसे
इतना रुक्ष नहीं रहना चाहूँगा।
मैं शायद उनसे यह सीखना चाहूँगा कि
हर गलत को युद्ध न बनाया जाए।
कुछ समझौते
जीवन को लंबा और
थोड़ा अधिक रहने योग्य बना देते हैं।
मैं यह भी सीखना चाहूँगा कि
नैतिकता को
कभी-कभी
मानव-संबंधों के पक्ष में झुकने दिया जाए।
यह कहना आसान नहीं है।
और कहना जोखिम भरा भी है।
पर सच शायद यही है।
5. कृष्णमोहन की सार्थकता
कृष्णमोहन की सार्थकता
उनके सही या गलत होने में नहीं है।
उनकी सार्थकता इस बात में है कि
वे मुझे
मेरी अपनी नैतिकता के बारे में
दोबारा सोचने पर मजबूर करते हैं।
वे मुझे यह याद दिलाते हैं कि
नैतिकता अगर
जीवन से कट जाए,
तो वह भी एक तरह का अहंकार बन सकती है।
मैं उनसे असहमत रहूँगा।
पर मैं उन्हें खारिज नहीं कर सकता।
और शायद
यही किसी व्यक्ति की
सबसे बड़ी विरासत होती है –
वह हमें
थोड़ा असहज छोड़ जाए।

“यह पोस्ट कृष्णमोहन पर नहीं है।
यह उस असहजता पर है
जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं,
जब किसी और का जीवन
हमारे अपने फैसलों से सवाल पूछ लेता है।”

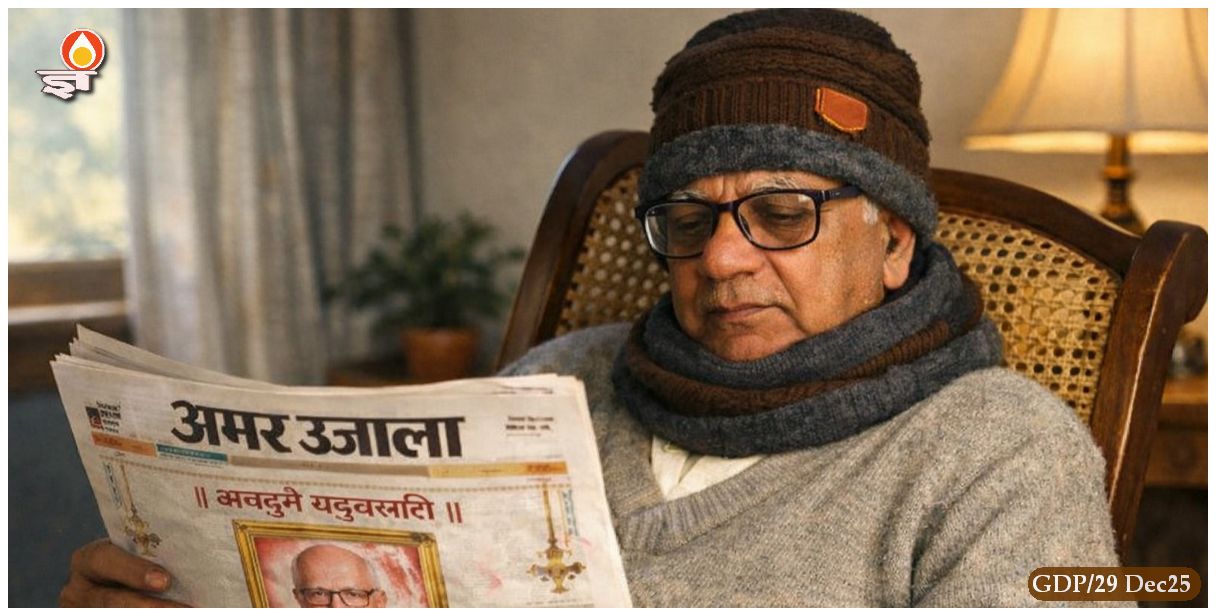
मैंने भी नौकरी में बहुत झेला क्योंकि मुझे लोगों को/अफसरों को खुश करना नहीं आता था। मेरे जमाने में मेरी वाली नौकरी में ठेकेदार के काम नहीं होते थे।होते भी तो मैं गंदा काम नहीं करवा पाता।मेरे अधीन गरीब लेबर से धन लेने की मैं सोच भी नहीं सकता था। तनख्वाह इतनी कम मिलती थी कि महिने के अंतिम सप्ताह में पैसे नहीं होते थे। जहां नौकरी करता था वहां का सामान बेचने की हिम्मत नहीं थी।बैरल भर पेट्रोल होता तो भी अपने स्कूटर में पंप पर जाकर पैसे देकर पेट्रोल भरवाता।
LikeLiked by 1 person
आपको संतोष तो होगा… 🙏
LikeLike