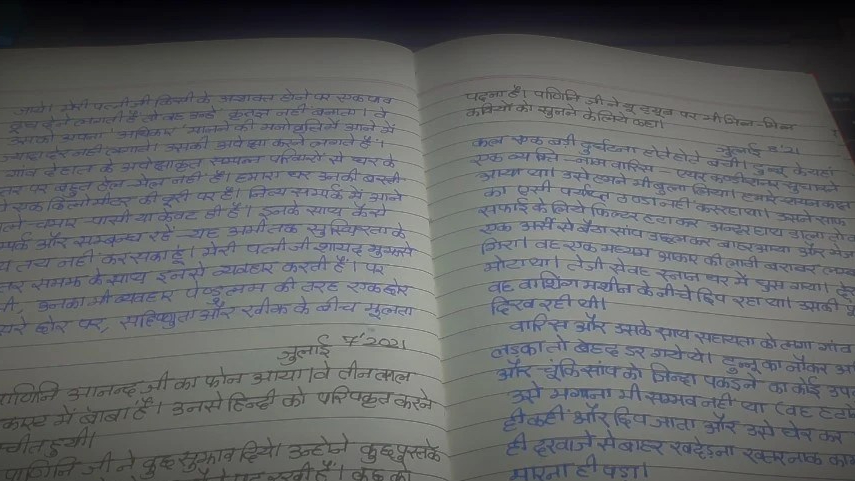मैं 1985 के उत्तरार्ध में जब अपनी पहली पोस्टिंग पर रतलाम रेल मण्डल में आया तो नीमच से गाजीपुर सिटी के लिये अफीम का लदान हुआ करता था। उस समय मेरी भूगोल के बारे में जानकारी सीमित थी। मुझे यह भी नहीं मालुम था कि नीमच से गाजीपुर में अफीम किस लिये जाती है। सोचता था कि शायद उस इलाके में लोग अफीम का सेवन ज्यादा करते हैं। नीमच में अफीम कहां से आती है, वह भी सही सही नहीं मालुम था। उस समय की सोचूं तो पाता हूं कि मेरे ज्ञान में तब से अब तक – चालीस साल में – जो कुछ बढ़ोतरी हुई है, वह एक क्रांति से कम नहीं। राज्य, देश, परदेश के बारे में अब मैं बहुत कुछ जानता हूं। और उससे आगे यह भी जानता हूं कि जो नहीं जानता उसे मिनटों, घण्टों में कैसे जाना जा सकता है। रेलवे की नौकरी, अपनी ज्ञानेंन्द्रियों को खुला रखने की आदत और इण्टरनेट ने मुझे वह सब बताया है जो मैं तब नहीं जानता था।
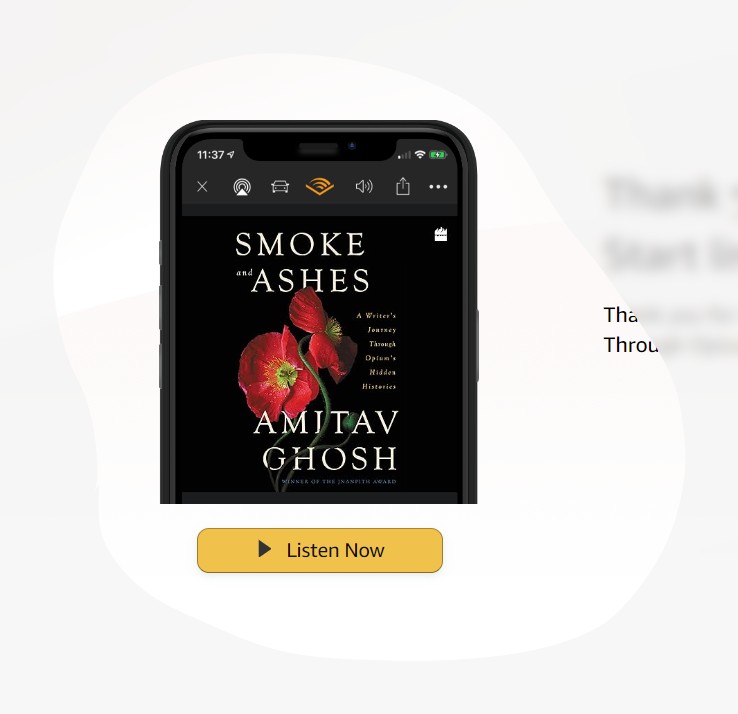
आज मैंने अमिताव घोष की पुस्तक – Smoke and Ashes: A Writer’s Journey Through Opium’s Hidden Histories का रिव्यू पढ़ा। पढ़ कर मैंने उसे ऑडीबल पर खरीद लिया। मुझे अंदाज है कि पांच सौ पेजों की यह किताब वैसे पढ़ना कठिन है। उसे साढ़े बारह घण्टे दे कर सुनना बेहतर विकल्प है। अमिताव घोष की इस किताब में अफीम के बारे में भारतीय परिदृष्य का ट्रेवलॉग, मेमॉयर और इतिहास का मिलाजुला प्रकटन है। मैं आशान्वित हूं कि यह मेरे काम की चीज होगी।
अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर की लड़ाई जीत कर पूर्वी भारत का अनाप-शनाप दोहन किया। जनता एक अकाल से दूसरे दुर्भिक्ष में झूलती रही। इसलिये जब लोग कहते हैं कि अंग्रेजों बदौलत भारत में नयी शिक्षा, सोच और रेल तथा दूर संचार आये; तब वे उसकी कीमत भूल जाते हैं जो हमारे देश ने भरी है। मेरे घर के आसपास नील की खेती से बंजर हुआ बड़ा गांगेय इलाका दीखता है। वह जमीन आज भी उर्वर नहीं हो पाई है। उसी तरह अफीम, पटसन आदि की खेती मनमाने तरीके से करा कर अंग्रेजों ने उत्तरप्रदेश, बिहार और झारखण्ड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो चौपट किया, वह आज भी इन प्रांतों की विपन्नता में नजर आता है।
उसके मुकाबले देश के पश्चिमी में, बम्बई से भीतरी भारत में अंग्रेजों की लिप्सा का निर्बाध प्रसार नहीं हुआ। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र में ग्वालियर, बड़ौदा, नागपुर, इंदौर के मराठों ने उन्हें वैसी मनमानी नहीं करने दी जैसे पूर्वी हिस्से में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने की। यहां के हिंदू, जैन, पारसी और मुस्लिम अफीम व्यापारियों ने भी उनके खुल्ले आतंक में ब्रेक लगाये। नीमच के आसपास अफीम की खेती से किसानों में खुशहाली और पूर्वी भाग में बदहाली का किस्सा मुझे अमिताव घोष की इस किताब से ज्यादा समझ आयेगा। और मैं चार दशक पहले के अपने रतलाम रेल मण्डल के अनुभवों को को-रिलेट कर सकूंगा।
अस्सी के दशक में रेलवे के वीपीयू (सवारी गाड़ी का पार्सल डिब्बा) में कच्चे अफीम का लदान हुआ करता था। नीमच से रतलाम तक छोटी लाइन (मीटर गेज) थी। रतलाम में अफीम का बड़ी लाइन में यानांतरण हुआ करता था। यहां से वीपीयू स्पेशल गाड़ी गाजीपुर सिटी के लिये जाया करती थी। उस स्पेशल में एक सवारी डिब्बा भी लगा होता था जिसमें अफीम की गार्ड और अन्य नार्कोटिक विभाग के कर्मचारी चला करते थे। यह स्पेशल गाड़ी रतलाम से उज्जैन, सिहोर, भोपाल के रास्ते जाती थी। मेरे रेल सेवा के शुरुआती दिनों में इसमें स्टीम इंजन लगता था। कालांतर में जब डीजल इंजनों की उपलब्धता बढ़ी तो डीजल इंजन भी लगाने लगे हम लोग। रतलाम रेल मण्डल में इस लदान से काफी आमदनी होती थी (रतलाम रेल मण्डल में वैसे मूल लदान बहुत ही कम होता था।) और हम इस स्पेशल को काफी तवज्जो दिया करते थे। पर फिर यह यातायात रेल से छिटक गया।
अफीम की तरह वीपीयू में लद कर देवास के बैंक नोट प्रेस से करेंसी की स्पेशल गाड़ी देश के कई हिस्सों में जाती थी। वह यातायात भी एक दशक बाद रेलवे से इतर चला गया। उस स्पेशल के बारे में तो मेरी हल्की सी स्मृति है कि रतलाम मण्डल पर ही कुछ लोगों ने (असफल) डकैती का प्रयास भी किया था। अखबारों में बहुत ज्यादा नहीं था उसके बारे में। ट्रेन के डिटेंशन की जानकारी से ही हमे पता चला था।

कच्चे अफीम के अलावा नीमच-मंदसौर से बहुत सा डोडा-चूरा वैगनों में लदान कर कलकत्ता के शालीमार स्टेशन जाता था। यह बल्क ट्रेफिक था। जगह ज्यादा घेरता था और उसका वजन कर होता था। मुझे कुछ लोग बताते थे कि डोडा-चूरा का प्रयोग वे चाय के साथ उबाल कर पीने में करते थे। उससे चाय का स्वाद बेहतर हो जाता है। मैंने इस प्रकार की चाय का कभी सेवन नहीं किया। मुझे भय लगता था कि कहीं अफीम की लत न लग जाये। वैसे उस पॉपी-हस्क में नशे जैसी कोई चीज नहीं थी ऐसा लोग बताते थे। पर व्यापारी शालीमार के लिये वैगनों की सप्लाई के लिये जिस प्रकार आपस में झगड़ते थे, उससे यह तो था कि इस चीज के व्यापार में काफी मुनाफा था। शायद इसकी प्रॉसेसिंग कर इससे भी अफीम की कुछ दवायें बनाई जाती हों।
मैंने कच्चे अफीम के लदान और परिवहन को काफी मॉनीटर किया पर कच्चा अफीम कभी देखा नहीं। अफीम के खेत में एक दो बार गया और उसके फल पर लगाया चीरा, जिससे निकलने वाले दूध को कांछ कर कच्चा अफीम बनता है, कई बार देखा।
रतलाम की वह ट्रेन परिचालन की नौकरी अब एक बार फिर करने का मौका मिले तो नये सिरे से बहुत कुछ जाना जा सकता है। पर वह सब होने से रहा। अब तो मुझे जानकारी पाने के लिये अमिताव घोष की पुस्तक ही सुननी-पढ़नी है।